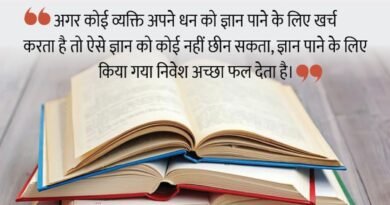राजनीति की बिगड़ती तस्वीर, धन कुबेरों और अपराधियों का बोलबाला !
criminals in politics यदि राजनीति में धन कुबेरों और अपराधियों का बोलबाला है तो उसे बदलेगा कौन? क्या देश की राजनीति में आमजन का कोई स्थान बचेगा? पंचायत से लेकर संसद तक एकसमान दृश्य है। कभी नेताओं के निर्माण के दो प्रमुख स्थल हुआ करते थे-छात्रसंघ और विभिन्न सामाजिक आंदोलन। समय के साथ ये दोनों मंच अप्रासंगिक होते गए।
…..प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ समय से राजनीति में युवाओं को लाने की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से अपने संबोधन में उन्होंने एक लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया था, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। इसी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर उन्होंने देश का भविष्य संवारने हेतु युवाओं को राजनीति में आने का पुनः आह्वान किया। इसका कारण क्या है? स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीतिक संस्कृति में ऐसी गिरावट आई कि लोग राजनीति को अवांछित तत्वों की शरणस्थली समझने लगे।
लोकतांत्रिक राजनीतिक-व्यवस्था में सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था एक विरोधाभास है। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताया था। आज कुछ नेता जो संविधान की प्रति लहराते हैं, वे सामंतवादी दलीय-व्यवस्था जीते हैं। वे परिवारवाद से ग्रस्त हैं और अपने दल एवं सरकार का नेतृत्व परिवार के अलावा किसी और को देना नहीं चाहते।
परिणामस्वरूप, पार्टियों में नए नेतृत्व, नई ऊर्जा का समावेश नहीं हो पा रहा है। अधिकतर दलों में सामंतवादी नेतृत्व है, जो अपने-अपने दलों को ‘कारपोरेट प्रतिष्ठानों’ के ‘सीईओ’ की तरह चलाते हैं। इससे राजनीतिक दलों में दूसरी पंक्ति के प्रभावशाली नेताओं का अभाव हो गया है। सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा खत्म होती जा रही है। केवल कुछ कैडर आधारित राजनीतिक दल ही इसमें अपवाद बचे हैं।
यदि लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण नहीं सुधरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, अच्छे नागरिकों का राजनीति में प्रवेश नहीं हुआ और नेताओं की नई पौध में अच्छे लोग नहीं आए तो फिर लोकतांत्रिक राजनीति के भविष्य पर सवाल उठेंगे। आखिर राजनीति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसे बदले? राजनीतिक दलों का चरित्र कैसे बदले? नेताओं की फसल कैसे बदले? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर देश को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये प्रश्न न केवल वर्तमान समाज, अपितु भावी-पीढ़ी और देश के भविष्य से भी जुड़े हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं तलाशने होंगे कि क्यों हम राजनीति को बुरा समझते हैं? यदि राजनीति बुरी होती तो कोई देश ऐसा होता, जहां राजनीति नहीं होती।
राजनीति के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक समाज की सुरक्षा एवं उसमें संघर्षों का समाधान और दूसरा लोककल्याण एवं विकास। यदि किसी समाज को इन लक्ष्यों को हासिल करना है तो उसे सुविचारित, बौद्धिक और जनहितकारी निर्णय लेने होंगे। क्या ऐसे निर्णय धनाढ्य और दागी जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए जा सकते हैं? इसके लिए तो समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग चाहिए, लेकिन ऐसे लोग ‘नौकरी’ को लक्ष्य बना लेते हैं और निर्णयन के सर्वोच्च स्तर अर्थात राजनीतिक निर्णयन के उत्तरदायित्व से बचते हैं। बचपन से ही उनके मन में रच-बस जाता है कि राजनीति बुरी है और यह उनके लिए नहीं है।
राजनीतिक दल तो लोकतंत्र के संवाहक हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष लोकतांत्रिक राजनीति के दो पहिये हैं। वे हमेशा रहेंगे, अलग रहेंगे, फिर भी एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे। अगर दलीय-पहिये खराब हो गए तो लोकतांत्रिक राजनीति की रेलगाड़ी चलेगी कैसे? राजनीतिक दलों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा, योग्य नेतृत्व और लोकतांत्रिक-संस्कृति जरूर है। इनके अभाव में योग्य और श्रेष्ठ युवा राजनीतिक दलों में नहीं आते। फलतः दलों का चारित्रिक ह्रास होता है।
उनमें नव-ऊर्जा का संचार नहीं होता। स्वस्थ और बौद्धिक विमर्श, जनाकांक्षा और जनहित के अनुरूप नीति-निर्धारण तथा दलीय-प्रदर्शन की निष्पक्ष समीक्षा नहीं होती। दल के सदस्य अपने नेतृत्व के उचित-अनुचित पर स्वतंत्र प्रतिक्रिया से बचते हैं और अपने नेता, दल और लोकतंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे में परिवारवादी और जातिवादी पार्टियों को अस्मितामूलक, संकुचित एवं बहिर्वेशी राजनीति छोड़कर विचारधारामूलक, समावेशी एवं आंतरिक-दलीय लोकतंत्र पर आधारित राजनीति की ओर अग्रसर होना चाहिए।
यदि राजनीति में धन कुबेरों और अपराधियों का बोलबाला है तो उसे बदलेगा कौन? क्या देश की राजनीति में आमजन का कोई स्थान बचेगा? पंचायत से लेकर संसद तक एकसमान दृश्य है। कभी नेताओं के निर्माण के दो प्रमुख स्थल हुआ करते थे-छात्रसंघ और विभिन्न सामाजिक आंदोलन। समय के साथ ये दोनों मंच अप्रासंगिक होते गए। छात्रसंघ एक तरह से उपद्रव संघ बन गए और उनकी प्रासंगिकता एवं गंभीरता समाप्त हो गई।
सामाजिक आंदोलनों से उपजे नेताओं ने क्षुद्र राजनीति कर अपनी जनस्वीकार्यता समाप्त कर दी। सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों के नेता अपने जीवनकाल में ही अप्रासंगिक हो गए। हाल में अन्ना हजारे अप्रासंगिक हो गए, लेकिन राजनीति को शुचितापूर्ण बनाए रखने के प्रयास की प्रासंगिकता आज और अधिक बढ़ गई है।
ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गैर-राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं को राजनीति से जोड़ने का आह्वान महत्वपूर्ण है। पार्टियां तो अपना प्रयास करेंगी ही, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को भी इसमें पहल करनी चाहिए। राजनीति से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, जो न केवल नई पीढ़ी से नेतृत्व तैयार करें, बल्कि राजनीति से जुड़ने वाले युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार भी खोलें।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं)