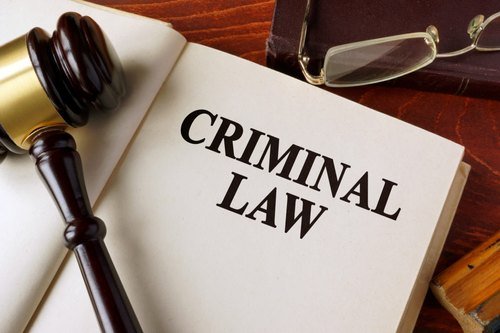120 दिन में IAS-IPS और दूसरे सिविल अफसरों पर मुकदमा चलाने की सहमति-असहमति देनी होगी
120 दिन में IAS-IPS और दूसरे सिविल अफसरों पर मुकदमा चलाने की सहमति-असहमति देनी होगी

आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिलों को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है। नए कानूनों में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित कई नए प्रावधान पेश किए गए हैं। नए कानूनों में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित कई नए प्रावधान पेश किए गए हैं। इतना ही नहीं, देश में अगर कोई सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस/आईपीएस या अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है, तो उस मामले में देरी नहीं होगी।
सक्षम अधिकारी या अथॉरिटी को इस मामले में मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। सिविल सर्वेंट्स के विरुद्ध प्रॉसिक्यूशन चलाने के लिए सहमति या असहमति पर सक्षम अधिकारी 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगा। यदि ऐसा न हो, तो यह मान लिया जाएगा कि अनुमति प्रदान हो गई है। सिविल सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य उसका प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर टेस्टीमनी दे सकेगा।
जांच की प्रगति को लेकर शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाएगा। पारंपरिक प्रचलन से हटकर पुलिस के लिए सख्ती से 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के संबंध में शिकायतकर्ता को बताना जरूरी है। न्यायिक क्षेत्र में दो चीजों पर बल दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया, सुनवाई में तेजी लाना और अनुचित स्थगन पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। धारा 392(1) में 45 दिनों के भीतर निर्णय की बात करते हुए मुकदमे को खत्म करने के लिए बेहतर ढंग से एक समयसीमा निर्धारित की गई है। न्याय में विलंब का अर्थ न्याय से वंचित होना है।
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रक्रिया बनाई जाएगी। क्राइम सीन से इन्वेस्टीगेशन और ट्रायल तक, सभी चरणों में टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। इसके माध्यम से पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा। विक्टिम और आरोपियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट तथा जजमेंट तक सभी डिजिटाइज्ड हो जायेंगे। सभी पुलिस थानों और न्यायालयों द्वारा एक रजिस्टर द्वारा ई-मेल एड्रेस, फोन नंबर अथवा ऐसा कोई अन्य विवरण रखा जाएगा। एविडेंस, तलाशी व जब्ती में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। इसे ‘अविलंब’ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की आवश्यकता है। पुलिस जांच के दौरान दिए गए किसी भी बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प रहेगा। सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में ‘फोरेंसिक एक्सपर्ट’ द्वारा क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन अनिवार्य होगा। वजह, इससे क्वॉलिटी ऑफ इन्वेस्टीगेशन में सुधार होगा। इन्वेस्टीगेशन साइंटिफिक पद्धति पर आधारित होगी और 100 फीसदी कन्विक्शन रेट का लक्ष्य पूरा होगा। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फॉरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी बनाया गया है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर फोकस किया गया है।
एनएफएसयू के कुल सात परिसर के अलावा 2 ट्रेनिंग अकादमी (गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, गुवाहाटी, भोपाल, धारवाड़) और सीएफएसएल पुणे एवं भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी की शुरुआत की जा रही है। चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन किया गया है।
पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया अथवा किसी संपत्ति का अधिगृहण करने में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग बिना किसी विलंब के संबंधित मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।
राज्य सरकार को एक पुलिस अधिकारी को नामित करने के लिए अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वह अधिकारी, सभी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी जानकारी को प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना भी आवश्यक है। छोटे-मोटे मामलों में समरी ट्रायल द्वारा तेजी लाई जाएगी।
कम गंभीर मामलों, चोरी, चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना अथवा रखना, घर में अनधिकृत प्रवेश, शांति भंग करने, आपराधिक धमकी आदि जैसे मामलों, के लिए समरी ट्रायल को अनिवार्य बनाया गया है। उन मामलों में जहां सजा 3 वर्ष (पूर्व में 2 वर्ष) तक है, मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज कारणों के अंतर्गत ऐसे मामलों में समरी ट्रायल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और वह एक तिहाई कारावास काट चुका है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जहां विचाराधीन कैदी ‘आधी या एक तिहाई अवधि’ पूरी कर लेता है, वहां जेल अधीक्षक अदालत को तुरंत लिखित में आवेदन दे। विचाराधीन कैदी को आजीवन कारावास या मौत की सजा में रिहाई उपलब्ध नहीं होगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन, इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेज, वेबसाइट व लोकेशनल साक्ष्य। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ‘दस्तावेज’ की परिभाषा में शामिल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान ‘साक्ष्य’ की परिभाषा में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए और अधिक मानक जोड़े गए हैं। इसके माध्यम से उचित कस्टडी-स्टोरेज-ट्रांसमिशन-ब्रॉडकास्ट पर जोर दिया गया है। दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति एवं एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने के लिए और अधिक प्रकार के माध्यमिक साक्ष्य जोड़े गए हैं। ये ऐसे साक्ष्य हैं, जिनकी जांच अदालत द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती है।
साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई। राज्य सरकार, एक एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करेगी और उसे नोटिफाईड भी करेगी। 10 वर्ष अथवा अधिक की सजा अथवा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा वाले मामलों में दोषी को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्डल ऑफेंडर) घोषित किया जा सकता है। घोषित अपराधियों के मामलों में, भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। पहले केवल 19 अपराधों में ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो सकते थे, अब इसमें 120 अपराधों को इस दायरे में लाया गया है। इसमें बलात्कार के अपराध को भी शामिल किया गया है, जो पहले शामिल नहीं था।