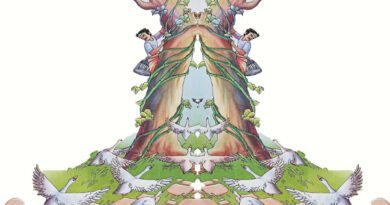सरकार की हदें भी तय करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ?
निजी संपत्ति का अधिग्रहण: बात दूर तलक जाएगी, सरकार की हदें भी तय करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों ने बहुमत से उनके हक में फैसला दिया है, पर चार दशक की मुकदमेबाजी के बाद आए इस फैसले से मकानमालिकों को कितनी राहत मिलेगी? अभी तक 17 मामलों में नौ जजों की संविधान पीठ बनी है। संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, दो या तीन जजों की पीठ मुख्य मामलों में फैसला सुनाती है। इसलिए इस फैसले के बाद भी लोगों को न्याय मिलने में और समय लग सकता है। दादा मुकदमा दायर करे, बेटा लडे़ और पोते के समय फैसला आए, लेकिन न्याय नहीं मिले। न्यायिक विलंब के इस देशव्यापी वायरस से मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगामी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
मुख्य फैसले से सहमत होने वाली जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए 130 पन्नों का अलग फैसला लिखा है। सनद रहे कि जस्टिस नागरत्ना कुछ साल बाद देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। वर्ष 1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था व्यक्तिगत जजों के व्यक्तिगत धारणाओं से ज्यादा बड़ी है। जस्टिस धूलिया के अनुसार, कृष्णा अय्यर के सिद्धांतों ने अंधकार भरे समय में देश का मार्गदर्शन दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जिस टिप्पणी से असहमति जताई, वह मुख्य फैसले में शामिल नहीं थी। लगता है कि ड्राफ्ट फैसले में बदलाव करके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी वाले अंश को हटा दिया था। यदि यह बात फैसला सुनाने से पहले जस्टिस नागरत्ना को बता दी जाती, तो असहमति के लंबे फैसले और न्यायिक जगत में चल रहे विवाद से बचा जा सकता था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अनुसार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के माध्यम से मान्यता मिली थी, लेकिन निजी संपत्ति पर लोगों के अधिकार और उसके अधिग्रहण के बारे में सरकार की सीमाओं पर आजादी के बाद से ही संसद और अदालत में विवाद चल रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों जैसे विषयों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के समय पहला संविधान संशोधन हुआ था। उसमे अनुच्छेद 31 में संशोधन करने के साथ नवमी अनुसूची शामिल की गई, जिसमें भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान था। भूमि सुधारों को लागू करने के लिए साल 1964 में 17वां संविधान संशोधन किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा सरकार ने संविधान में 25वां और 42वां संशोधन किया। जनता पार्टी की सरकार ने साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300-ए के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया, लेकिन इस पूरी कवायद से सिर्फ यह फर्क पड़ा कि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है।
कई संविधान संशोधन व अदालत के फैसलों के बाद कुछ बातें साफ हो गईं। पहला, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति का अधिकार सांविधानिक अधिकार है। अधिग्रहण की प्रक्रिया को सिर्फ कानून के शासन के दायरे में निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए संपत्ति का अधिकार अप्रत्यक्ष तौर पर संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दूसरा लोकहित में सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, पर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन कर मुआवजा देना जरूरी है। नोटिस, सुनवाई और लिखित आदेश के बगैर चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक और नया फैसला उल्लेखनीय है। उसके अनुसार अवैध निर्माण हटाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। तीसरा अनुच्छेद 39-बी के मुताबिक, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के संसाधनों को इस तरह से बांटे कि वे सभी की भलाई के काम आएं, लेकिन इसके लिए सभी निजी संपत्ति के अधिग्रहण और नियंत्रण का सरकार को अधिकार नहीं है। अब निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन के योग्य मानने के पहले अनेक परीक्षण करने के साथ कानून से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का पूरा पालन जरूरी होगा। आर्थिक संसाधनों के समान वितरण के लक्ष्य को पाने के लिए संपत्ति पर जनता के सांविधानिक अधिकारों के साथ संतुलन बनाना जरूरी है।
इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अभी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नजीर माना जाए, तो आर्थिक उदारवाद और बाजारवाद को न्यायिक मान्यता मिलने से उस मामले की सुनवाई भी नौ या ज्यादा संख्या जजों की पीठ द्वारा होनी चाहिए। यूपीए और एनडीए, दोनों सरकारों को भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून बनाने और लागू करने में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले और स्पष्टीकरण से महाराष्ट्र के अलावा, दूसरे राज्यों के कानून पर भी असर पड़ेगा और यह तय होगा कि सरकार कब और किस हद तक निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।