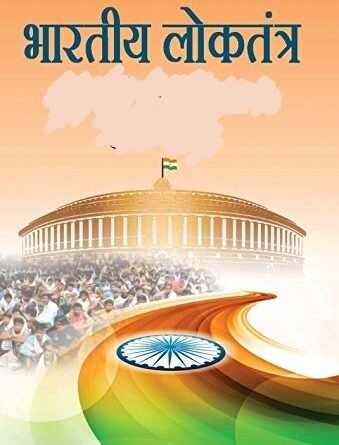लोकतंत्र किसके लिए?
सत्ता में छिपा हुआ एक स्वार्थ होता है, जो उसके अंहकार तथा एक तरफा निर्णय का कारण होता है। जहां सत्ता निरंकुश तक स्वच्छंद हो जाए, वहां जनता के नाम से सत्ताधारियों का हित साधन करने में लग जाती है। आज सरकारें पूर्ण मनोयोग से इसी एक सूत्री कार्यक्रम में जुटी हैं। सारी नई योजना की परिणति सरकारों-नेताओं और अधिकारियों का ही सुख बढ़ा रही है। चाहे शहर की सफाई का ठेका हो, चाहे गरीबों की आवास योजनाएं, सब कुछ ठेके पर नीलाम होता है। राजमार्गों तक की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और मंत्री को इन्हें देखने की फुर्सत तक नहीं। छोटे उद्योग लगाने के आंकड़ों में उलझाकर बेरोजगारों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को खाद बांटने में भारी अफरातफरी मची है और मंत्री अपने रिश्तेदारों की जेबें भरने में जुटे हैं। मंत्रियों के जोर पर बिल्डर बड़ी-बड़ी रकम खा रहे हैं। जंगलों पर मंत्रियों ने कब्जे कर रखे हैं। कागज तो कुछ भी बन जाते हैं।
दूसरा सत्य है कि कोई भी मंत्री या नेता बिना-अधिकारियों की मदद के कुछ कर नहीं सकता। फाइलें सब इनके हाथ में जो होती हैं। कई मंत्रियों को अंग्रेजी नहीं आती, कई को मुद्दे ही व्यापक स्तर पर समझ में ही नहीं आते। कई सारे लेन-देन अधिकारियों से ही करवाते हैं। तब वे अपनी मजदूरी क्यों नहीं मागेंगे! आज सरकार को चुनती तो जनता है, किन्तु जनता के हित में कार्य नहीं करती। जनता के बीच आती तक नहीं। कभी अधिकारीगण सामाजिक कार्यक्रमों में विशिष्ट रूप से बुलाए जाते थे। आज ब्याज पर धन लगाते हैं।
समय के साथ दो नए परिवर्तन आए। राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की भर्तियां रोक रखी हैं अथवा संविदा पर कार्य होता है। अधिकारियों की न भर्तियां रुकीं, न वेतन वृद्धियों तथा पेंशन में अंतर आया। जिस विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी था वहां अब 7-8 हो गए। कितनी क्षमता बढ़ी होगी। फिर भी सरकार को अधिकारियों की तो कमी लगती है, कर्मचारियों की नहीं। किसी को यह भी समझ नहीं कि कितना कमाना चाहते हैं और क्यों! इतनी बड़ी राशि खर्च भी कहां करें। झक मार कर माफिया को देना पड़ता है, बाहर भेजना पड़ता है अथवा तितर-बितर। भोग नहीं सकते-नष्ट होती है, देश को भी नष्ट करती है। उनके चले जाने के बाद भी नष्ट ही करेगी।
शिक्षा लेना सिखाती है। सत्ता में जिसकी लाठी, उसकी भैंस! जो बड़े पद पर, वहां बड़ी मलाई। मंत्री भी विधायक और दूसरा विधायक भी साधारण विधायक। फिर खाने में इतना अन्तर! कैसे सहन हो? बस आज सारी कसरत इस ईर्ष्या देवी के कारण चल रही है। दो गुटों में सरकार-बड़ी मछली-छोटी मछली। तीसरा है विपक्ष। सरकारी खजाना बड़ी मछलियों के पास, दलाली सरकार के पास, रिश्वत छोटी मछलियों के पास। छीनाझपटी के नजारे भी कई जगह माया की कलाकारी पेश करते हैं।
नेताओं और अफसरों के बीच तू-तू-मैं-मैं भी होने लगी है। संतुष्टि किसी स्तर पर नहीं है। सबको ‘और चाहिए’। एक लोकप्रिय स्लोगन सुना होगा-‘ये दिल मांगे मोर’।
उसके लिए एक राजनीतिक मुद्दा बना-नए जिले बनाने को। आबादी बढ़ गई, विकास की परिभाषाएं बदल गईं। नए स्थानीय स्कूल-कॉलेज-अस्पतालों की आवश्यकता भी बढ़ गई। नेताओं, विशेषकर स्थानीय नेताओं के लिए यह ‘बिल्ली के भाग छींकां’ हुआ। अफसरों को नए पद, नई स्थानीय व्यवस्थाएं आदि मूल कारण बन गए। राजस्थान निर्माण के समय जहां 25 जिले थे, आज 33 हैं। एक-एक जिले पर सैंकड़ों करोड़ मासिक के वेतन-भत्तों का खर्च जुड़ता है। इससे पेट नहीं भरा तो संभाग बनाकर आयुक्त बना दिए। सन् 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। सन् 1987 में स्वर्गीय हरदेव जोशी ने अजमेर जोड़कर पुन: छह संभाग बना दिए। बाद में वसुन्धरा सरकार ने 2005 में एक और सातवां संभाग-भरतपुर घोषित कर दिया। धौलपुर 1982 में 27 वां जिला बना। अप्रेल 91 में दौसा, बारां और राजसमंद – तीन जिले जोड़े गए। 2008 में हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ को जिले घोषित कर 33 कर दिए गए। आज लगभग 80 नए जिले बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास हैं।
नए जिले बनाना समय की आवश्यकता भी है। राजस्थान बना, तब जनसंख्या दो करोड़ थी। आज आठ करोड़ है। इसके आधार पर नए परिसीमन की आवश्यकता पड़ने वाली भी है। अन्य राज्यों से राजनीतिक स्पर्धा होती है। आज छत्तीसगढ़-तेलंगाना जैसे राज्यों में ही 33-33 जिले हैं। मध्यप्रदेश में 52, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। विधायकों एवं सांसदों की संख्या का आधार भी बदला जाता है। चुनावी खर्चे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो क्षेत्रफल बड़ा है, आबादी उतनी नहीं।
आज राजस्थान में 250 आइएएस, 190 आइपीएस और 900 आरएएस अधिकारी हैं। कुछ 13 लाख कर्मचारी हैं। इनके वेतन और पेंशन पर लगभग 7000 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होते हैं। विकास की दर और वास्तविकता विकास का आकलन नहीं दिखाई देता है। आज तो हम बराबर पीछे जा रहे हैं। इन तथ्यों का वास्तविक आकलन किया जाता। राजनीतिक दृष्टि और चुनाव जीतने का लक्ष्य ही आधार होता है। क्या कोई सरकार दावा कर सकती है कि बारां, राजसमंद और दौसा आज भी जिलों की तरह विकसित हो चुके हैं। आज भी ये कोटा, उदयपुर और जयपुर पर आश्रित दिखाई देते हैं। केवल सरकारी तंत्र का और नेताओं का बोलबाला हुआ है। खर्चे के अनुपात में विकास शून्य बराबर हुआ। प्रदेश के औसत विकास से भी कम है। आज ब्यावर, पचपदरा, भिवाड़ी, बालोतरा जैसे कस्बे इनसे कहीं आगे हैं। करौली तो हिण्डौन से भी पीछे है।
कमोबेश यही हाल मध्यप्रदेश का भी रहा है। वहां 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तब सात नए जिले बने थे-बडवानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, हरदा और नीमच। सन् 2013 में शाजापुर के दो जिले बनाकर आगर-मालवा बनाया। सन् 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग किया। पिछले 24 वर्षों में वहां भी नौ जिले तो बन गए, जनता को इसका लाभ कुछ नहीं हुआ। जनता के सिर नया बोझ ही पड़ा। इसका दर्द किसके दिल में है? सारा खेल आंकड़ों और अफसरों का ही है। जो अतिरिक्त भार जनता पर पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन? जिन नेताओं ने स्वीकृति दी, वे तो भूल भी गए होंगे।
सब कुछ होते हुए भी नए जिलों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। बनने भी चाहिए। सेवाओं का विस्तार होता है। स्वास्थ्य-शिक्षा-न्याय जैसी सुविधाओं का विकास भी उतना ही आवश्यक है। फिर भी नए जिले बनाने से पहले पुराने जिलों के विकास एवं भावी संभावनाओं का वास्तविक आकलन होना चाहिए। जो नए जिले नाकारा साबित हुए, उनके पुनर्गठन पर भी विचार हो। राजनीति आधार नहीं हो। जातिगत आधार पर लोकतंत्र को खतरा है। इस पर स्वतंत्र तथ्यों -प्राकृतिक संसाधन-रेल-उद्योग आदि के आधार पर निर्णय हो। कई शहर आज भी जिलों से आगे हैं, ऐसे में उनको जिला बनाकर पुनर्गठन किया जा सकता है। कुछ जिलों को अनावश्यक, निरर्थक मानकर निर्णय किया जाए, तो कुछ को आबादी के हिसाब से।
पिछले चार साल में औद्योगिक विकास भी नगण्य हुआ। भले ही कोविड का बहाना हो। बिजली, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य जैसे विभागों ने भी अलग-अलग ढंग से सरकार की नाक ही कटाई। योजनाओं की जमीनें भी ठेकों पर बेचकर, नशीले पदार्थों के आवागमन की छूट देकर, अतिक्रमण की बढ़ती गति की अनदेखी कर, अपराधियों के साथ पुलिस की सांठगांठ को बढ़ावा देकर सरकार जमीन से दूर हो गई। सरकार कोई हो, अफसर वही होते हैं। अत: नए जिलों की कार्यप्रणाली बदलेगी, संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशयल इन्टेलीजेंस जैसी तकनीक के उपयोग को, केन्द्रीय नियंत्रण के विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखकर नए निर्णय होने चाहिए। यदि किसी अधिकारी का कार्यक्षेत्र पिछड़ता है, समय पर योजना पूरी नहीं होती, तो जवाबदेही के तौर पर कार्रवाही होनी चाहिए। किसी को तीस लाख की रिश्वत देते, समाचार छपवाते तो देख सकते हैं,किन्तु रिश्वत लेने वाले को पूरी छूट है। अर्थात सरकार अधिकारियों के आगे कठपुतली है। इस स्थिति में जिले हों या न हों, राज तो अफसरों को ही करना है। नेता शाम को गल्ला संभालते रहें। हमारा लोकतंत्र इन्हीं देशभक्तों पर आश्रित है। नए जिलों से छोटे नेताओं को भी मंत्रियों जैसा सम्मान तो मिलेगा। अपनी हुकुमत तो चला पाएंगे। हां, गरीब और गरीब होता चला जाएगा।
उसके लिए एक राजनीतिक मुद्दा बना-नए जिले बनाने को। आबादी बढ़ गई, विकास की परिभाषाएं बदल गईं। नए स्थानीय स्कूल-कॉलेज-अस्पतालों की आवश्यकता भी बढ़ गई। नेताओं, विशेषकर स्थानीय नेताओं के लिए यह ‘बिल्ली के भाग छींकां’ हुआ। अफसरों को नए पद, नई स्थानीय व्यवस्थाएं आदि मूल कारण बन गए। राजस्थान निर्माण के समय जहां 25 जिले थे, आज 33 हैं। एक-एक जिले पर सैंकड़ों करोड़ मासिक के वेतन-भत्तों का खर्च जुड़ता है। इससे पेट नहीं भरा तो संभाग बनाकर आयुक्त बना दिए। सन् 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। सन् 1987 में स्वर्गीय हरदेव जोशी ने अजमेर जोड़कर पुन: छह संभाग बना दिए। बाद में वसुन्धरा सरकार ने 2005 में एक और सातवां संभाग-भरतपुर घोषित कर दिया। धौलपुर 1982 में 27 वां जिला बना। अप्रेल 91 में दौसा, बारां और राजसमंद – तीन जिले जोड़े गए। 2008 में हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ को जिले घोषित कर 33 कर दिए गए। आज लगभग 80 नए जिले बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास हैं।
नए जिले बनाना समय की आवश्यकता भी है। राजस्थान बना, तब जनसंख्या दो करोड़ थी। आज आठ करोड़ है। इसके आधार पर नए परिसीमन की आवश्यकता पड़ने वाली भी है। अन्य राज्यों से राजनीतिक स्पर्धा होती है। आज छत्तीसगढ़-तेलंगाना जैसे राज्यों में ही 33-33 जिले हैं। मध्यप्रदेश में 52, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। विधायकों एवं सांसदों की संख्या का आधार भी बदला जाता है। चुनावी खर्चे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो क्षेत्रफल बड़ा है, आबादी उतनी नहीं।
आज राजस्थान में 250 आइएएस, 190 आइपीएस और 900 आरएएस अधिकारी हैं। कुछ 13 लाख कर्मचारी हैं। इनके वेतन और पेंशन पर लगभग 7000 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होते हैं। विकास की दर और वास्तविकता विकास का आकलन नहीं दिखाई देता है। आज तो हम बराबर पीछे जा रहे हैं। इन तथ्यों का वास्तविक आकलन किया जाता। राजनीतिक दृष्टि और चुनाव जीतने का लक्ष्य ही आधार होता है। क्या कोई सरकार दावा कर सकती है कि बारां, राजसमंद और दौसा आज भी जिलों की तरह विकसित हो चुके हैं। आज भी ये कोटा, उदयपुर और जयपुर पर आश्रित दिखाई देते हैं। केवल सरकारी तंत्र का और नेताओं का बोलबाला हुआ है। खर्चे के अनुपात में विकास शून्य बराबर हुआ। प्रदेश के औसत विकास से भी कम है। आज ब्यावर, पचपदरा, भिवाड़ी, बालोतरा जैसे कस्बे इनसे कहीं आगे हैं। करौली तो हिण्डौन से भी पीछे है।
कमोबेश यही हाल मध्यप्रदेश का भी रहा है। वहां 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तब सात नए जिले बने थे-बडवानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, हरदा और नीमच। सन् 2013 में शाजापुर के दो जिले बनाकर आगर-मालवा बनाया। सन् 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग किया। पिछले 24 वर्षों में वहां भी नौ जिले तो बन गए, जनता को इसका लाभ कुछ नहीं हुआ। जनता के सिर नया बोझ ही पड़ा। इसका दर्द किसके दिल में है? सारा खेल आंकड़ों और अफसरों का ही है। जो अतिरिक्त भार जनता पर पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन? जिन नेताओं ने स्वीकृति दी, वे तो भूल भी गए होंगे।
सब कुछ होते हुए भी नए जिलों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। बनने भी चाहिए। सेवाओं का विस्तार होता है। स्वास्थ्य-शिक्षा-न्याय जैसी सुविधाओं का विकास भी उतना ही आवश्यक है। फिर भी नए जिले बनाने से पहले पुराने जिलों के विकास एवं भावी संभावनाओं का वास्तविक आकलन होना चाहिए। जो नए जिले नाकारा साबित हुए, उनके पुनर्गठन पर भी विचार हो। राजनीति आधार नहीं हो। जातिगत आधार पर लोकतंत्र को खतरा है। इस पर स्वतंत्र तथ्यों -प्राकृतिक संसाधन-रेल-उद्योग आदि के आधार पर निर्णय हो। कई शहर आज भी जिलों से आगे हैं, ऐसे में उनको जिला बनाकर पुनर्गठन किया जा सकता है। कुछ जिलों को अनावश्यक, निरर्थक मानकर निर्णय किया जाए, तो कुछ को आबादी के हिसाब से।
पिछले चार साल में औद्योगिक विकास भी नगण्य हुआ। भले ही कोविड का बहाना हो। बिजली, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य जैसे विभागों ने भी अलग-अलग ढंग से सरकार की नाक ही कटाई। योजनाओं की जमीनें भी ठेकों पर बेचकर, नशीले पदार्थों के आवागमन की छूट देकर, अतिक्रमण की बढ़ती गति की अनदेखी कर, अपराधियों के साथ पुलिस की सांठगांठ को बढ़ावा देकर सरकार जमीन से दूर हो गई। सरकार कोई हो, अफसर वही होते हैं। अत: नए जिलों की कार्यप्रणाली बदलेगी, संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशयल इन्टेलीजेंस जैसी तकनीक के उपयोग को, केन्द्रीय नियंत्रण के विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखकर नए निर्णय होने चाहिए। यदि किसी अधिकारी का कार्यक्षेत्र पिछड़ता है, समय पर योजना पूरी नहीं होती, तो जवाबदेही के तौर पर कार्रवाही होनी चाहिए। किसी को तीस लाख की रिश्वत देते, समाचार छपवाते तो देख सकते हैं,किन्तु रिश्वत लेने वाले को पूरी छूट है। अर्थात सरकार अधिकारियों के आगे कठपुतली है। इस स्थिति में जिले हों या न हों, राज तो अफसरों को ही करना है। नेता शाम को गल्ला संभालते रहें। हमारा लोकतंत्र इन्हीं देशभक्तों पर आश्रित है। नए जिलों से छोटे नेताओं को भी मंत्रियों जैसा सम्मान तो मिलेगा। अपनी हुकुमत तो चला पाएंगे। हां, गरीब और गरीब होता चला जाएगा।