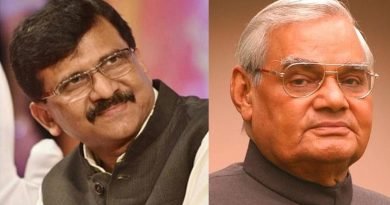संसदीय सीटों के परिसीमन पर मच रहा है बवाल !
84वां संवैधानिक संशोधन, परिसीमन और उत्तर-दक्षिण की उबलती राजनीति
संविधान का 84वां संशोधन
इस टॉपिक को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं – क्या है 84वां संवैधानिक संशोधन, डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, और ये साउथ इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहले बात करते हैं 84वें संवैधानिक संशोधन की. ये 2001 में पास हुआ था, और इसके तहत डिलिमिटेशन प्रोसेस पर एक तरह की रोक लगा दी गई. डिलिमिटेशन माने क्या? आसान भाषा में – संसद और स्टेट असेंबली की सीटों को दोबारा अरेंज करना, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से हर इलाक़े को सही रिप्रेजेंटेशन मिले. लेकिन 84वें अमेंडमेंट ने डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी मतलब अभी तक जो सीटें हैं, वो फिक्स रहेंगी. ये फैसला 42वें संशोधन (1976) से चला आ रहा था, जिसमें 1971 की जनगणना को बेस बनाकर सीटें फ्रीज़ की गई थीं. फिर 84वें संशोधन ने इस फ्रीज़ को 2026 तक बढ़ा दिया.
अब सवाल ये है – ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब है फैमिली प्लानिंग. उस वक़्त गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करें. जो स्टेट्स इसमें कामयाब होंगे, उन्हें इनाम मिलेगा – उनकी सीटें कम नहीं होंगी. लेकिन जो स्टेट्स फेल होंगे, उनकी सीटें बढ़ सकती हैं. साउथ इंडिया के स्टेट्स – जैसे आंध्र, तमिल नाडु, केरला – ने इस पॉलिसी को सीरियसली लिया. नतीजा? इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई. दूसरी तरफ, नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में पॉपुलेशन बूम होता रहा. 2011 की सेंसस के मुताबिक़ साउथ स्टेट्स का देश की टोटल पॉपुलेशन में शेयर 1971 से कम हो गया. जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि पिछले 15 साल में ये शेयर और घटा होगा.
डिलिमिटेशन का डर
साउथ इंडिया की टेंशन बढ़ रही है क्योंकि अब डिलिमिटेशन का टाइम नज़दीक आ रहा है. 84वां संशोधन 2026 में ख़त्म होगा, और उसके बाद नई सेंसस (जो शायद 2026 में होगी) के बेस पर सीटें री-अरेंज होंगी. साउथ स्टेट्स को डर है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है. उदाहरण के लिए, अगर यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहां की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, लेकिन तमिल नाडु या आंध्रा की सीटें घट सकती हैं. ये साउथ के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि संसद में उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी.जगन रेड्डी ने अपनी चिट्ठी में यही पॉइंट उठाया. उनका कहना है कि साउथ स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को दिल से फॉलो किया. नेशनल प्रायोरिटी थी, तो इन्होंने मेहनत की. लेकिन अब इनकी सजा मिलेगी? ये तो नाइंसाफी है! वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन ऐसा हो कि किसी स्टेट की सीटों का शेयर कम न हो. इसके लिए वो संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं – ख़ास तौर पर आर्टिकल 81(2)(a) में. उनका सुझाव है कि हर स्टेट की सीटें प्रोपोर्शनली बढ़ें, ताकि साउथ को लॉस न हो और नॉर्थ को भी फायदा मिले.पॉलिटिक्स का खेल – कौन क्या चाहता है?
ये मसला सिर्फ़ टेक्निकल नहीं, बल्कि पॉलिटिकल भी है. साउथ के लीडर्स को लगता है कि अगर सीटें पॉपुलेशन बेस्ड हुईं, तो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी. बीजेपी, जो नॉर्थ में स्ट्रॉंग है, को फायदा हो सकता है. दूसरी तरफ, साउथ की पार्टियाँ – जैसे वाईएसआरसीपी, डीएमके, टीआरएस – इसको अपने ख़िलाफ़ देख रही हैं. तमिल नाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तो चेन्नई में ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ताकि सब मिलकर इस पर स्ट्रैटेजी बनाएँ. लेकिन जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई. फिर भी, जगन ने लेटर लिखकर अपनी बात रखी.वाई वी सुब्बा रेड्डी ने ये लेटर डीएमके को भी भेजा, ताकि साउथ की पार्टियाँ एकजुट हों. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जगन का स्टैंड थोड़ा अलग है. वो डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि ये “फेयर” हो. स्टालिन और बाकी साउथ लीडर्स शायद इसे पूरी तरह रोकना चाहते हैं. ये पॉलिटिकल ड्रामा अभी और चलेगा, क्योंकि 2026 नज़दीक आते ही दबाव बढ़ेगा. इतिहास में देखे तो मालूम होता है की डिलिमिटेशन कोई नई चीज़ नहीं है. इंडिया में ये पहले भी कई बार हुआ – 1952, 1963, 1973, और 2002 में. हर बार सेंसस के बाद सीटें अरेंज की गईं. लेकिन 42वें और 84वें संशोधन ने इसे फ्रीज़ कर दिया. मक़सद था कि स्टेट्स फैमिली प्लानिंग पर फोकस करें. लेकिन 2011 की सेंसस ने साबित कर दिया कि सब स्टेट्स एक जैसे रिज़ल्ट नहीं दिखा पाए.
परिवार नियोजन का प्रभाव
साउथ ने कंट्रोल किया, नॉर्थ में पॉपुलेशन बढ़ता रहा. अब सवाल ये है – क्या 2026 के बाद भी फ्रीज़ को बढ़ाना चाहिए? या डिलिमिटेशन को नया फॉर्मूला देना चाहिए?सॉल्यूशन क्या हो सकता है?जगन रेड्डी का आइडिया बुरा नहीं है. अगर सीटें प्रोपोर्शनली बढ़ें, तो बैलेंस बना रहेगा. लेकिन ये आसान नहीं. लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं. अगर नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी, तो टोटल सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी. संसद का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, जो लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली चैलेंजिंग है. दूसरा ऑप्शन है की फ्रीज़ को 2031 तक बढ़ा दिया जाए, जैसा कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं. लेकिन ये सिर्फ़ टाइम खरीदने की बात होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी.एक और रास्ता है – डिलिमिटेशन का बेस सिर्फ़ पॉपुलेशन न हो. इसमें डेवलपमेंट, कॉन्ट्रिब्यूशन टू नेशनल जीडीपी, और एजुकेशन जैसे फैक्टर्स भी शामिल किए जाएँ. साउथ स्टेट्स का तर्क है कि वो टैक्स में ज़्यादा योगदान देते हैं, तो उनकी आवाज़ कमज़ोर क्यों हो? ये डिबेट अभी खुली है, और इसका जवाब ढूंढना गवर्नमेंट के लिए टफ टास्क होगा. ये डिलिमिटेशन का मसला सिर्फ़ नंबर्स का खेल नहीं है. ये पावर, रिप्रेजेंटेशन, और फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है. साउथ इंडिया की टेंशन जायज़ है, क्योंकि उनकी मेहनत की सजा नहीं मिलनी चाहिए. जगन मोहन रेड्डी ने सही मुद्दा उठाया, लेकिन सॉल्यूशन इतना आसान नहीं. 2026 तक का टाइम नज़दीक आ रहा है, और तब तक पॉलिटिक्स का धुआँ और गरम होगा. ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके देश की राजनीती में दूरगामी नतीजे होंगे,सर्कार को साउथ इंडिया की पोलिटिकल पार्टीज़ के चिंता को अड्रेस करने की ज़रूरत है.