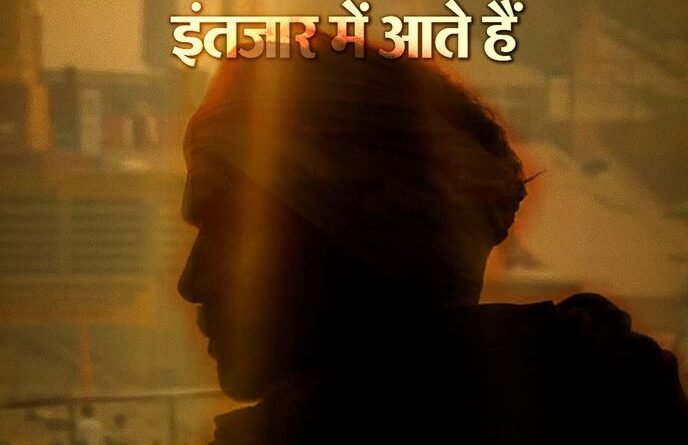वो इमारत, जहां 15 दिन में उखड़ जाती हैं सांसें ….?
10 कमरे अब तक 14 हजार से ज्यादा मौतों के गवाह बने….
छोटा था, तबसे लेकर अब तक हजारों मौतें करीब से देखीं। लोगों के आंगन में पक्षी चहचहाते हैं। हमारे यहां मौत चहलकदमी करती। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर के कंपाउंड में आते-आते ही किसी ने देह छोड़ दी। यहां हर कमरे की सफेद दीवार के पीछे मौत की स्याही है।
गलियों की भूलभुलैया और पान-ठंडाई की खुशबू वाली वाराणसी में जैसे ही गिरिजाघर चौराहे पर पहुंचेंगे, एक खास गंध लपककर आपका हाथ थाम लेगी। ये है मौत की गंध। कुछ ही मीटर की दूरी तय करने पर काशी लाभ मुक्ति भवन है। वो दुमंजिला इमारत, जहां के 10 कमरे अब तक 14 हजार से भी ज्यादा मौतें देख चुके।
इमारत की देखरेख करने वाले अनुराग शुक्ल कहते हैं- आखिरी सांसें ले रहा शख्स अगर मुंहमांगे पैसे देकर भी किसी पांच सितारा होटल में रहना चाहे तो भी कमरा नहीं मिलेगा। मरते हुए आदमी को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। काशी में मोक्ष खोजते आए ऐसे ही लोगों का ठौर है मुक्ति भवन। अब तक 14 हजार 878 लोग मौत से मुलाकात के लिए यहां आ चुके, और सिलसिला जारी है।
लकड़ी के हरे दरवाजों और सफेद दीवारों से घिरी, साल 1908 में बनी ये इमारत अपने-आप में कहानी है। यहां के हर कमरे में मौत का इंतजार बसता है।

ऐसे ही किस्सों की तलाश में जब हम मुक्ति भवन पहुंचे, उससे कुछ ही घंटों पहले एक शख्स का मोक्ष हुआ था। कमरा साफ-सुथरा होकर दूसरे मोक्षार्थी की बाट जोह रहा था। यहां लकड़ी के दो तखत पड़े हुए थे। एक मरीज के लिए, दूसरा परिवार के लिए। दीवारें एकदम खाली और सफेद, सिर्फ एक कैलेंडर फड़फड़ा रहा था।
पुराने ढब से बने इस कमरे में लकड़ी की खिड़कियां हैं, जो ज्यादातर बंद रहती हैं, कि कहीं आती हुई मौत, मौका पाकर निकल न भागे।
इस पर मुक्ति भवन के व्यवस्थापक अनुराग शुक्ल कहते हैं- वाकई ऐसा होता है! कई बार एंबुलेंस या गाड़ी भवन के भीतर घुसती है और मरीज को मोक्ष मिल जाता है। वहीं कई ऐसे लोग भी आते हैं, जिनके चेहरों पर मौत की सफेदी पुती होती है। वे रात-रातभर दर्द से बेहाल रहते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए शरीर पर घाव हो जाता है, लेकिन मर नहीं पाते। तब उन्हें लौटना पड़ता है।

दरअसल भवन का नियम है कि यहां किसी को 15 दिनों के लिए ही कमरा मिलता है। इस वक्त तक अगर को मोक्ष न मिल सके तो उसे बाहर जाना होता है। कभी-कभार ये भी होता है कि हालत देखकर 15 दिनों की मियाद बढ़ा दी जाती है। ये वो लोग होते हैं, जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। जिनका शरीर धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहा होता है। जो खाना-पीना लगभग छोड़ चुके होते हैं। और जिनकी आंखों में मौत का इंतजार टिमटिमाता होता है।

कैसा होता है ऐसे घर में रहना, जहां जिंदगी की रौनक कम, मौत का शोर ज्यादा हो?
इस पर अनुराग कहते हैं- पढ़ाई के दिनों में मुश्किल होती थी। मित्र-दोस्त डरते कि अनुराग जहां रहता है, वहां रोज या हर दूसरे-तीसरे दिन अर्थी उठती है। मैं सबके घर जाता, लेकिन कोई मेरे घर नहीं आता था। जन्मदिन अकेले मनाता। तब बहुत तकलीफ होती थी। वक्त के साथ समझ आया कि ये भवन आखिरी इच्छा लिए कितने ही लोगों का आखिरी ठिकाना है। फिर तकलीफ खत्म हो गई।
दुख तो चला गया, लेकिन तब भी पूरी तरह से मुक्ति भवन से जुड़ नहीं सका था। कहने को यहीं रहता। कभी गाड़ी, कभी एंबुलेंस की आवाज सुनता, रोते-बिलखते लोग दिखते, लेकिन कहीं कुछ दूरी थी। मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता था। उसी की पढ़ाई की और प्रैक्टिस भी करने लगा। तभी साल 2018 में एकाएक पिताजी गुजर गए और भवन संभालने का जिम्मा मुझ पर आ गया।
मैंने काला कोट उतार दिया और मुक्ति भवन का बंदोबस्त देखने लगा। तब से लगातार मौतों का गवाह बन रहा हूं।

पूरी बातचीत के दौरान अनुराग मौत की जगह मोक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो भी इतनी सहजता से, जैसे खाने के मेन्यू की बात हो रही हो।
मैं पूछती हूं- रोज-रोज अपने ही अहाते से अर्थी निकलते देख तकलीफ नहीं होती? जवाब आता है- दुख तो होता है, लेकिन परिवारवालों को देखकर। वे खुद ही अपने परिजन को यहां लेकर आते हैं। खुद ही उसकी आसान मौत की प्रार्थना करते हैं, लेकिन मौत के बाद सबसे ज्यादा दुखी भी वही होते हैं। कोई कितना भी तैयार क्यों न हो, मौत सबको झकझोरकर ही जाती है।
अनुराग के बाद हमारी मुलाकात होती है, यहीं काम करते काली दुबे से। फुर्ती से चलने और उतनी ही तेजी से बोलने वाले काली मोक्षार्थियों की जरूरतें भी पूरी करते हैं और सुबह-शाम खूब खुली हुई आवाज में भजन भी गाते हैं।
जब हम पहुंचे, वे बगीचे की गुड़ाई-निराई कर रहे थे। हाथ रोककर बात शुरू की तो बताते ही चले गए। कहते हैं- काशी जगह ही ऐसी है, जहां मौत से आप ऐसे मिलते हैं, मानो दोस्त से मिल रहे हों। धौल-धप्पा होगा, थोड़ी गपशप होगी और फिर वो आपका हाथ पकड़कर ले जाएगी।

सालों से यहां हूं। जैसे ही किसी एंबुलेंस की आवाज आती है, लपककर दरवाजे पर जाता हूं। वहां मोक्षार्थी की हालत देखी जाती है, इसके बाद ही एंट्री मिलती है। अगर कोई सेहतमंद है तो वो यहां कमरा नहीं छेक सकता। अगर कोई अकेला है, तो भी उसे यहां रहने नहीं मिलेगा। जैसे कुछ रोज पहले ही एक शख्स आया, जो आखिरी दिन यहां बिताना चाहता था। अकेला देखकर हमें उसे लौटाना पड़ा। जाते हुए उसकी बूढ़ी आंखें भरभरा गई थीं। उसे देखकर तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन यही नियम है।
मुक्ति भवन में बातचीत के बाद मैं बाहर निकलने को तैयार होती हूं। लोहे का मेन दरवाजा 45 डिग्री की गर्मी में भी एकदम ठंडा था, मानो मौत उसे भी छूकर निकली हो।
गिरिजाघर चौराहे से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है मर्णिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहां चौबीसों घंटे चिताएं जलती रहती हैं। शायद सच ही हो क्योंकि जब मैं पहुंची, सामने ही आठ चिताएं जल रही थीं। घाट पर यहां-वहां बिखरे परिवारवाले सिसक रहे थे। कोई तसल्ली देते हुए खुद रो रहा था। पास ही में वो जगह थी, जहां चिता के लिए लकड़ियां दी जाती हैं।

लकड़ियां तुलवा रहे राहुल चौधरी डर या दुख के मेरे सवाल पर कहते हैं- बचपन से मसान में रहे। चिता जलने के बाद जो लकड़ियां बच जाएं, वो हम अपने चूल्हे में डाल देते हैं। दान के अन्न से खाना पकाते हैं। चिता के कपड़े खुद भी पहन लेते हैं। हमें मौत से डर नहीं लगता, हां तकलीफ जरूर होती है।
कोई जवान लाश जलने के लिए आती है तो लकड़ी तुलवाते हुए हथेली पसीज जाती है। कोई बच्चा जलता है तो पसीना पोंछने के बहाने हम भी आंसू पोंछते हैं।
तब भी कभी तो डर लगा होगा? सवाल दोहराने पर जवाब आता है- हां, कोरोना के समय बहुत डर लगा था। पॉलिथीन में बंद लाशें आतीं। अच्छे-खासे परिवारवाले अनाथों की तरह अकेले मसान पहुंच रहे थे। बच्चे अपने मरे हुए मां-बाप से भाग रहे थे। इतनी लाशें जलीं कि कोई हिसाब नहीं। हर बार लगता कि अगली बारी हमारी होगी, लेकिन कुछ इंसानियत और कुछ आदत ने सब करवा दिया।