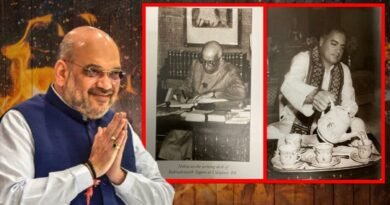शहरों-जगहों के नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है हमारी महान विरासत को अंगीकार करना
देश में जगहों, शहरों, सड़कों के नाम बदलने की परिपाटी नई नहीं है। यह आजादी के बाद से ही चली आ रही है। एक स्वतंत्र देश को यह अधिकार है कि वह अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत पर दावा पेश करे। लेकिन हाल ही में मुगल गार्डंस का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया जाना मेरी दृष्टि में अवांछनीय था। क्योंकि भले ही बाबर 1526 में उज्बेकिस्तान से भारत आया हो, लेकिन ब्रिटिशों के उलट मुगल अनेक सदियों की प्रक्रिया में धर्मबहुल, विविधतापूर्ण भारत की बुनावट में घुल-मिल गए थे। वहीं विलियम मस्टो नामक जिन होर्टिकल्चरिस्ट ने मुगल गार्डंस की रचना की थी, उन्होंने वैसा मुगलों के परम्परागत बागों के पैटर्न पर किया था।
लेकिन यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जगहों के नाम बदलने के अलावा हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने को और क्या जतन किए हैं? हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी औपनिवेशिक सांचे में ही संचालित होती है, इसमें अंग्रेजों के जमाने से अब तक नाममात्र का बदलाव आया है। हमारी इतिहास-पुस्तकों को अनुपयुक्त तरीके से लिखा गया है।
मिसाल के तौर पर विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेवराय या राजराजा चोल प्रथम को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र या महाभारत के शांतिपर्व में वर्णित राजनीतिक अंतर्दृष्टियों के अध्ययन के लिए बहुत थोड़े प्रयास हुए हैं। भक्तिकाल छह शताब्दियों तक चला था और इस दौरान भक्तिधारा का श्रेष्ठतम काव्य रचा गया, लेकिन हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम में इसे बहुत मामूली स्थान दिया जाता है।
दर्शनशास्त्र के विभागों में भारतीय सभ्यता के महान योगदान को परिधि पर सीमित कर दिया जाता है, वहां आज भी पश्चिमी चिंतकों का बोलबाला है। बहुत सारे लोगों को जैमिनी, कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि, शंकर जैसे दार्शनिकों की मेधा के बारे में पता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की विलक्षण उपलब्धियों का हमारे शैक्षिक कोर्स में लगभग कोई उल्लेख नहीं होता।
विज्ञान की पढ़ाई में भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों के योगदान की अवहेलना की जाती है। पाणिनी के अष्टाध्यायी समेत व्याकरण, शब्द-व्युत्पत्ति, भाषाशास्त्र के अनेक ग्रंथों की उपेक्षा कर दी जाती है। हमारे एलीट स्कूलों में शेक्सपीयर का नाम सबने सुना है, लेकिन कालिदास को बामुश्किल ही किसी ने पढ़ा होगा। हमारी एयरलाइंस में भी केवल अंग्रेजी भाषा के अखबारों को ही जगह दी जाती है।
रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को हमारी शैक्षिक कल्पना में स्थान नहीं मिलता। तुलसीदास और तिरुवल्लुर की अंतर्दृष्टियों को दरकिनार कर दिया जाता है। चार आश्रम, गीता का निष्काम कर्म, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के पुरुषार्थों पर अकादमिक गम्भीरता से संवाद नहीं किया जाता। आर्किटेक्चर की पढ़ाई में वास्तुशास्त्र को स्थान नहीं दिया जाता।
200 ईस्वी पूर्व में लिखा गया भरतमुनि का नाट्यशास्त्र- जो कि कलाओं पर दुनिया का सम्भवतया पहला इतना विस्तृत ग्रंथ है- भी लगभग अल्पज्ञात है। सौंदर्यशास्त्र के छात्रों को रस-परिपाक की जानकारी नहीं होती। हमारा सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुनियोजित नहीं है। देश में विश्वस्तरीय ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल का अभाव है।
यहां तक कि दिल्ली का सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम भी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। हमारे ऐतिहासिक स्मारक शोचनीय दशा में हैं। संग्रहालयों की पूछ-परख करने वाला कोई नहीं। वहां उपयुक्त डिस्प्ले, कैटेलॉगिंग का अभाव होता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और नेशनल म्यूजियम में चंद हजार ही लोग आते हैं। इसकी तुलना में न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और पेरिस के लूव्र में सालाना 25 लाख लोगों की आमद होती है, वहीं लंदन के टेट में 40 लाख लोग आते हैं।
लेकिन इस सबके लिए संसाधनों की जरूरत होती है। 2019-20 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया व्यय हमारी जीडीपी का मात्र 0.012 प्रतिशत था। 2021 में संस्कृति मंत्रालय को 451 करोड़ रुपए दिए गए, जो विगत वर्ष के आवंटन से 15 प्रतिशत कम थे।
यह तब है, जब 2020 के सांस्कृतिक बजट का साल के मध्य में रिवीजन करके उसे 30 प्रतिशत कम कर दिया गया और ताजा बजट में उसमें मामूली बढ़ोतरी ही की गई। संक्षेप में कहें तो संस्कृति हमारी प्राथमिकता में नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोश भी अब लगभग निष्क्रिय हो गया है।
2019-20 में संस्कृति मंत्रालय का व्यय हमारी जीडीपी का मात्र 0.012 प्रतिशत था। 2020 के सांस्कृतिक बजट का साल के मध्य में रिवीजन करके उसे 30 प्रतिशत कम कर दिया गया था। संस्कृति हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)