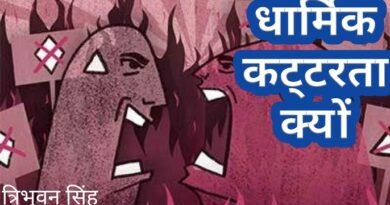पसीने के पार असह्य हुई गर्मी ?
पसीने के पार असह्य हुई गर्मी, अब वैश्विक उष्मन एक नये दौर में
इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक की आयोजन समिति ने एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल के बिना ही पूरे खेल के आयोजन का फैसला किया है. इसके मूल में कम से कम उर्जा के इस्तेमाल से इस बड़े वैश्विक आयोजन को संपन्न करने का लक्ष्य है. हालांकि, फ्रांस के इस निर्णय के खिलाफ कई विकसित देशों ने अपने खिलाड़ियों के लिए अलग से वैकल्पिक एयर कंडीशनिंग मुहैया कराने की पेशकश की है. वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भीषण गर्मी झेल रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक स्थानीय उपभोक्ता अदालत की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिसके पास एयर कंडीशनर या कूलर नहीं था. मई महीने से ही भीषण गर्मी से आम जन के प्रभावित होने यहां तक हताहत होने की खबरें संपूर्ण उत्तर भारत में आम हो चली है. पूर्वी राज्य बिहार में कई छात्र हीटस्ट्रोक से बेहोश हो गए, जिसके बाद सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई. ये दोनों परिस्थितियां दो अलग-अलग कहानी कह रही है, पर दोनों के मूल में वैश्विक उष्मन के नए दौर में बढती गर्मी का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ही है, यानी गर्मी का मौजूदा दौर एक नयी ऊंचाई छू रहा है, जो मानव के गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता से आगे की परिस्थिति है.
तापमान छू रहा नयी ऊंचाई
कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज के मुताबिक पिछला महीना और पिछला साल अब तक का क्रमशः सबसे गर्म मई महीना और सबसे गर्म साल साबित हुआ है, जिसका असर समूचे पृथ्वी के ऊष्मा विन्यास पर पड़ा है. समुद्र से लेकर ग्लेशियर और महाद्वीप धीरे-धीरे ही सही गर्म हो रहे हैं. पाकिस्तान, भारत सहित दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अरब, पश्चिमी अफ्रीका से लेकर मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका तक में तापमान नयी ऊंचाई छू रहा है. हीटवेव की चपेट से यूरोप के देश भी अछूते नहीं है. भारत में तो अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जब दिल्ली में थर्मामीटर ने 50° सेल्सियस को पार कर लिया, हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने इसे तकनीकी मसला मान लिया, पर फिर भी दिल्ली के कई इलाकों का तापमान दो-तीन दिनों तक 49°सेल्सियस के आसपास बना रहा. उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में तापमान मई के मध्य से ही 45° सेल्सियस के आसपास बना हुआ है.
मौजूदा भीषण गर्मी के पीछे स्थानीय मौसमी परिस्थितियां जिसमें वायु का दबाब,आर्द्रता, समुद्र से दूरी, भूमि का उपयोग आदि शामिल है, के अलावा मानव जनित वैश्विक उष्मन का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है. वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन द्वारा किए गए विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है कि पश्चिमी अफ्रीका में गर्मी की लहर का होना मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बिना “लगभग असंभव” था और भारत सहित अन्य क्षेत्रों में फैलता हीट-वेव का दायरा लगभग उसी तर्ज पर है. वैश्विक उष्मन के कारण स्थानीय और वैश्विक स्तर के मौसमी परिस्थितियां तापमान को तेजी से बढा रहे हैं, जिसमें लगातार ‘उच्च दबाब’ का बना रहना जिसे ‘हीट डॉम’ भी कहते है, अल नीनो की तीव्रता और अनियमित होना, मानसून का अनियमित होना आदि शामिल है.
तापमान में बेतहाशा वृद्धि
जैसा कि विदित है कि गर्मी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें ना सिर्फ तापमान बढ़ा है, जिसका मापन परम्परागत रूप से सतह से थोड़ी ऊंचाई पर हवा के तापमान से पता चलता है, बल्कि बढ़ी गर्मी में सामान्य थर्मामीटर का पारा इस बात को व्यक्त करने में नाकाम है कि बढ़ी हुई गर्मी को हम कैसे महसूस करते हैं? हमारा शरीर बढती गर्मी को कैसे बर्दाश्त करता है? इस तापमान और मानव शरीर पर हुए उसके असर को समझने में तापमान के अलावा वातावरण में मौजूद नमी की मात्रा एक महत्वपूर्ण अवयव है. जिसकी महत्ता वैश्विक उष्मन के दौर में अचानक से समझ आने लगी है. मानव शरीर का बढ़ते तापमान को सहन करने की क्षमता को समझने के लिए हवा के तापमान और हवा में मौजूद आर्द्रता की मात्रा के बीच के सम्बन्ध को समझना जरुरी है.
गर्मी से शरीर पर भी प्रभाव
पक्षी सहित मानव का शरीर समतापी होता है यानी शरीर एक खास तापमान को हमेशा बनाकर रखता है और इस उपार्जन में हवा में मौजूद नमी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है. मनुष्यों की दो पैरों पर चलने की क्षमता, नग्न त्वचा और पसीने की ग्रंथियां एक परिष्कृत शीतलन प्रणाली बनाती हैं. जब वातावरण का तापमान शरीर के तापमान से ज्यादा होता है तो शरीर से पसीना निकलता है जो हवा के संपर्क के आकर वाष्प बन जाता है और इस प्रक्रिया में वाष्प आसपास से ढेर सारी ऊष्मा (गुप्त ऊष्मा) सोख लेता है. जब आसपास से ढेर सारी ऊष्मा पसीने के वाष्प बनने के क्रम में सोख ली जाती है तब जाहिर सी बात है कि शरीर ठंडा हो जाता है और आरामदेह महसूस होता है.
जब तापमान और ज्यादा होता है तब पसीने के साथ-साथ खून का फैलाव शरीर की बाहरी परत यानी त्वचा के आस-पास होने लगता है, ताकि पसीने के वाष्पन से खून का तापमान भी कम हो और इस प्रकार शरीर के आंतरिक अंगों का तापमान नियंत्रण में रहता है. हवा में मौजूद नमी या आर्द्रता शरीर से होने वाले पसीने की दर को नियंत्रित करती है. किसी खास तापमान पर जब वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होती है, तो शरीर से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, यानी पसीना कम निकलता है. इसके विपरीत उसी तापमान पर जब हवा में नमी कम रहती है, तब अपेक्षाकृत पसीने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर से वाष्पीकरण ज्यादा होता है. अगर तापमान और आर्द्रता दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो पानी की उपलब्धता के साथ छाया में बैठा एक स्वस्थ व्यक्ति भी गर्मी की चपेट में आ जाएगा.
नमी के साथ बढ़ता हीट इंडेक्स
यह स्पष्ट है कि शुष्क परिस्थितियों में शरीर वास्तव में ठंडा महसूस करता है, वहीं आर्द्र परिस्थितियों में गर्म महसूस करता है. शायद इसी कारण से आम बोलचाल में कहा जाता है कि ‘ये गर्मी नहीं है, ये नमी है’ और समुद्र के तटीय इलाकों में भले तापमान कम हो पर गर्मी हो जाती है, जिसे चिपचिपी गर्मी कहते हैं. हवा के तापमान के साथ मौजूद नमी से पता चलता है कि हमारा शरीर इस तापमान पर कैसा महसूस करता है. तापमान और नमी को एक साथ हीट इंडेक्स के रूप में निरुपित करते हैं. हवा में नमी के साथ हीट इंडेक्स बढ़ता है, यदि दो जगह हवा का तापमान समान भी हो तो जहां नमी कम होगी वहां हमें अपेक्षाकृत ज्यादा आराम महसूस होगा, यानी हीट इंडेक्स कम होगा.
हीट इंडेक्स हवा के तापमान से इतर वह आभासी तापमान है जो हमारा शरीर महसूस करता है. तभी जब स्मार्ट फोन पर मौसम का हाल देखते हैं तो दो तापमान दिखता है. पहला तापमान हवा का तापमान होता है और दूसरा तापमान जो हमारा शरीर महसूस करता है,जो हवा के तापमान से आजकल अक्सर बहुत ज्यादा होता है. मानेसर में 13 मई 2024 को दिन दो बजे तापमान 44.1° सेल्सियस, सापेक्षित आर्द्रता 28% और 50.6° सेल्सियस महसूस हो रहा तापमान था, जो असल में हीट इंडेक्स है. 44.1° सेल्सियस का तापमान अगर सापेक्षित आर्द्रता 28% हो तो यह हमारे शरीर पर 50.6° सेल्सियस जैसा असर कर रही होगी.
खतरनाक स्थिति में है प्रकृति
ग्रह पर हमारे अस्तित्व के सैकड़ों हज़ारों वर्षों में,हमने कई तरह की जलवायु के साथ तालमेल बिठाने में कामयाबी हासिल की है, सहारा रेगिस्तान की शुष्क गर्मी से लेकर आर्कटिक की बर्फीली ठंड तक हम झेलते हैं, लेकिन वैश्विक उष्मन के दौर में गर्मी का दायरा और तीव्रता दोनों तेजी से बढ़ रही है. मनुष्य के शरीर की परिष्कृत शीतलन प्रणाली के बावजूद पृथ्वी का बढ़ता तापमान हाल के कुछ वर्षों में सबसे खतरनाक प्राकृतिक खतरे के रूप में उभरकर सामने आयी है. विषुवतीय क्षेत्र के अलावा यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में बढ़ रही हीट स्ट्रोक की घटनाएं इस बात की तस्दीक करती है. पिछले दस सालों में भीषण गर्मी और आर्द्रता के काकटेल से दसियों हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है.
वो अलग बात है कि भारत में अभी भी हीटवेव से उपजी आपदा को आपदा के रूप में नहीं माना जाता. गर्मी और आर्द्रता के योगात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से ना सिर्फ मानव स्वास्थ्य पर आसन्न खतरे के रूप में सामने आया है बल्कि आम मानव कार्य क्षमता को प्रभावित कर बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधि को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया है. जिसमें कृषि, भवन और मुलभूत संरचना निर्माण, औद्योगिक उत्पादन मुख्य रूप से शामिल हैं. ऐसे में जरुरत है कि ना सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक उष्मन के लक्ष्य पर समग्रता से प्रयास किया जाये. जाहिर है कि इसका फ़िलहाल कोई समाधान वर्तमान विकास के प्रारुप में नहीं दिखता है और ना ही तमाम देशों की इच्छा-शक्ति में दिखता है, चाहे हम कितना ही हो हल्ला मचा दें.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि … न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.