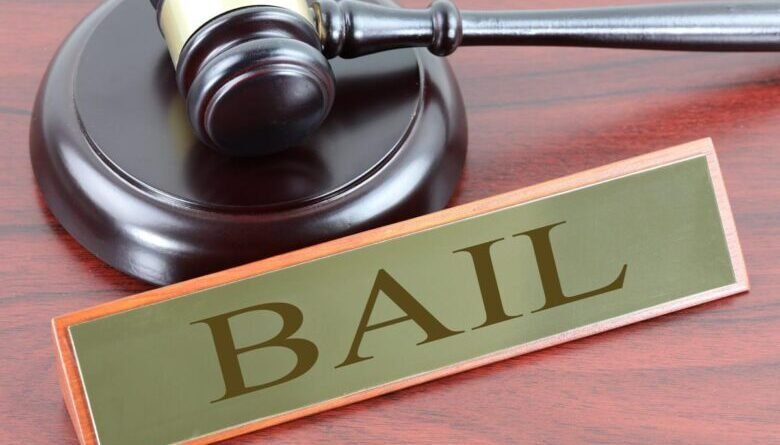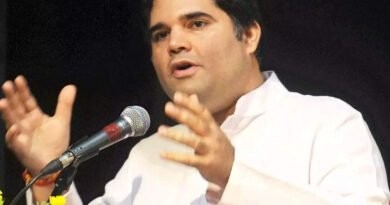हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, जमानत पर जोर दें
हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, जमानत पर जोर दें
सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। जमानत-सम्बंधित कानूनों पर ताजा चर्चा एक नेता के अभियोजन के संदर्भ में उठी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जमानत पर शीघ्र ट्रायल के मौलिक अधिकार पर बल दिया।
पीठ ने जांच में देरी के लिए ईडी एवं सीबीआई की कठोर शब्दों में निंदा की। 17 महीनों की कैद के बाद सिसोदिया रिहा हुए। तीन सप्ताह बाद उनकी सह-आरोपी भारत राष्ट्र समिति की सांसद के कविता को भी जमानत दे दी गई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई अन्य आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं।
कहते हैं कि गठबंधन सरकार के दौरान न्यायपालिका अधिक सक्रिय होती है। तो अब यह पूछने का समय है कि आने वर्षों में जमानत-सम्बंधित कानून में क्या बदलाव आएगा। इस संदर्भ में विशेष रूप से तीन क्षेत्र रुचि के होंगे : मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) जैसे ‘विशेष कानूनों’ के तहत जमानत; सामान्य प्रतिवादियों की जमानत पर लगाई जाने वाली शर्तों का विनियमन; और कानून में स्थिरता लाने के लिए संभावित संसदीय कदम।
पीएमएलए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 जैसे विशेष कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिसोदिया के मामले में पीएमएलए की धारा 45 पर विवाद था, जो जमानत आवेदनों का ट्विन टेस्ट अनिवार्य बनाती है : 1. जमानत देने के लिए न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी जमानत पर बाहर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा और 2. यह मानने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह दोषी नहीं है।
सिसोदिया के मामले में, न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया कि इस धारा की व्याख्या इस तरह से न हो कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ की जानी-पहचानी कहावत को नकार दिया जाए। इस कदम के बावजूद, पीएमएलए की धारा 45 या यूएपीए की धारा 43 डी(5) जैसे कठोर प्रावधानों के तहत स्वतंत्रता की समर्थक न्यायिक मंशा को बनाए रखना मुश्किल है।
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 45 को विजय मदनलाल चौधरी के मामले में 2022 में संवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायपालिका का जमानत के प्रति हृदय-परिवर्तन कितना सच्चा है, यह इस फैसले पर पुनर्विचार की कसौटी पर कसेगा।
मनीष सिसोदिया के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद गिरीश गांधी बनाम गुजरात राज्य के मामले में एक और आदेश आया, जिसमें न्यायमूर्ति गवई और विश्वनाथन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया। उसमें जमानत देने के लिए कठोर शर्तें रखी गई थीं, खास तौर पर स्थानीय जमानतदारों की आवश्यकता के संबंध में। न्यायमूर्तियों ने कहा कि अत्यधिक कठोर शर्तों के तहत जमानत देना जमानत न देने के ही समान है।
यदि न्यायमूर्ति के शब्दों का पालन किया जाए तो हम शेख अयूब जैसे मामलों को दोहराने से बच सकते हैं। शेख अयूब को ढाई लाख रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने जमानत शर्त भी ढाई लाख रुपयों की रखी और 50000 रुपए का प्रतिभूति बंधपत्र भी मांगा, यानी जितने के गबन का आरोप था, उससे अधिक पैसे जमानत मिलने में लग जाते। हालांकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन शर्तों को रद्द कर दिया था। लेकिन ऐसे अनेक मामले भारत के सत्र न्यायालयों में देखे जाते हैं।
पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, भारत में जमानत की स्थिति को अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी के उच्च आदर्शों के साथ जोड़ना कठिन होगा। इस अधिकार को बार-बार संकुचित किया गया है।
न्यायपालिका ने अब रास्ता सुझाया है। कार्यपालिका में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन दशक पहले जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में बताया था कि गिरफ्तारी की शक्ति केवल पुलिस को जांच में सहायता देने के लिए है। हर मामले में गिरफ्तारी का इस्तेमाल जरूरी नहीं।
विधायिका को सतेंद्र अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में न्यायालय के आह्वान को स्वीकार कर व्यापक जमानत कानून तैयार करना चाहिए। जमानत पर बहस अमूमन हाई-प्रोफाइल मामलों से प्रेरित होती है। फिर भी कानून के इस क्षेत्र को स्पष्ट करने के इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। राजनीति के अपराधीकरण का समाधान फौजदारी कानून का राजनीतिकरण नहीं हो सकता।
अपराधियों को दोषी ठहराना चाहिए और उन्हें सजा भी काटनी चाहिए, लेकिन आरोपी को प्रक्रिया से प्रताड़ित करने का कोई अर्थ नहीं। जमानत-सम्बंधित कानून में सुधारों को आपराधिक प्रक्रिया में सुधार की शुरुआत माना जाना चाहिए।
(ये लेखकों के अपने विचार हैं।)